संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन विभिन्न SSC परीक्षाओं, जैसे SSC CGL, CHSL, MTS और अन्य SSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं में समान महत्व रखते हैं। इस अनुभाग में उत्कृष्टता प्राप्त करने में आपकी सहायता के लिए, हम भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधनों पर आवश्यक नोट्स पेश कर रहे हैं। संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन अर्थात् संविधान के अनुभाग से संबंधित किसी भी आशंका को दूर करने में यह लेख आपकी मदद करेगा।
भारतीय संविधान
भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पिछले कुछ वर्षों में, संविधान में कई बदलाव और परिवर्धन हुए हैं, जिन्होंने इसे हमारे देश के लिए अधिक व्यापक और प्रासंगिक बना दिया है। आइए इस लेख में नीचे भारतीय संविधान में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों पर चर्चा करें।
संविधान की मूल संरचना
- भारतीय संविधान की मूल संरचना आवश्यक समझे जाने वाले मूल सिद्धांतों के एक समूह को संदर्भित करती है, जिसे संसद द्वारा संशोधनों के माध्यम से नष्ट या बदला नहीं जा सकता है। यह अवधारणा, हालांकि संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले (1973) में स्थापित की गई थी।
- बुनियादी संरचना का सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति पर एक जांच है और यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के मौलिक लोकाचार, सिद्धांत और अंतर्निहित ढांचा इसकी भावना को संरक्षित करते हुए बरकरार रहे।
भारतीय संविधान में संशोधन के प्रकार
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों का प्रावधान करता है:
- संसद के विशेष बहुमत द्वारा (सदन की कुल सदस्यता का 50% + उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य),
- संसद के विशेष बहुमत तथा साधारण बहुमत द्वारा 1/2 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा,
- एक अन्य प्रकार का संशोधन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है।
- हालाँकि, इन संशोधनों को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संशोधन नहीं माना जाता है।
- इसलिए, संविधान में तीन तरीकों से संशोधन किया जा सकता है:
- संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन,
- संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और
- संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा
भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन
भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन नीचे सारणीबद्ध हैं।
| संशोधन | वर्ष | विवरण |
|---|---|---|
| प्रथम संशोधन | 1951 | मौखिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और जमींदारी उन्मूलन कानूनों के सत्यापन के साथ मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में संशोधन किया। |
| द्वितीय संशोधन | 1952 | लोकसभा के चुने गए सदस्य के लिए निर्धारित जनसंख्या सीमा को हटा दिया। |
| तृतीय संशोधन | 1954 | सातवें कार्यसूची में विधायी सूची में संशोधन किया। |
| चौथा संशोधन | 1955 | संपादन किए गए धारा 31 और 31A, जिससे संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के मुआवजे और नौवें कार्यसूची पर प्रभाव पड़ा। |
| पांचवां संशोधन | 1955 | केंद्र सरकार द्वारा संदिग्ध मामलों पर राज्यों के विचार व्यक्त करने के लिए समय सीमा जोड़ी गई। |
| छठा संशोधन | 1956 | सातवें कार्यसूची में संशोधन किया और कर नियामक संबंधित धाराओं में परिवर्तन किया। |
| सातवां संशोधन | 1956 | राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू करने के लिए व्यापक परिवर्तन लाए। |
| आठवां संशोधन | 1959 | निश्चित समुदायों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों की आरक्षण को बढ़ाया। |
| नवां संशोधन | 1960 | भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के तहत निश्चित क्षेत्रों को पाकिस्तान को स्थानांतरित किया। |
| दसवां संशोधन | 1961 | नि:शुल्क दादरा और नगर हवेली को भारत संघ में एकीकृत किया। |
| ग्यारहवां संशोधन | 1962 | उपराष्ट्रपति के चुनाव को संविधानिक मंडल के बजाय संसद की संयुक्त बैठक द्वारा लाए गए। |
| बारहवां संशोधन | 1962 | गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों को भारत संघ में सम्मिलित किया। |
| तेरहवां संशोधन | 1962 | नागालैंड राज्य की स्थापना की। |
| चौदहवां संशोधन | 1963 | पुडुचेरी के पूर्व फ्रांसीसी क्षेत्र को संघ में सम्मिलित किया। |
| पंद्रहवां संशोधन | 1963 | उच्च न्यायालय न्यायियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से 62 वर्षों तक बढ़ाया और न्यायियों के नियमों के व्याख्यान को यथार्थीकरण करने के लिए छोटे संशोधन किए गए। |
| अठारहवां संशोधन | 1966 | पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने, पंजाब और हरियाणा में विभाजन को सुगम बनाने और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बनाने में सहायता प्रदान की। |
| इक्यावीं संशोधन | 1967 | आठवें कार्यसूची में सिंधी को 15वें क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया। |
| बावें संशोधन | 1969 | असम के भीतर मेघालया का एक उप-राज्य बनाया गया। |
| तेईसवें संशोधन | 1969 | SC/ST के लिए सीटों की आरक्षण और एंग्लो-इंडियन की नियुक्ति को और 10 वर्षों तक बढ़ाया गया (1980 तक)। |
| छब्बीसवें संशोधन | 1971 | राजकीय राज्यों के पूर्व शासकों के शीर्षकों और विशेष विशेषाधिकारों को खत्म किया। |
| सत्तावें संशोधन | 1971 | मणिपुर और त्रिपुरा के राज्यों की स्थापना की और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी के रूप में गठित किया गया। |
| इकतीसवें संशोधन | 1973 | लोकसभा के चुने गए सदस्यों की चुनावी संख्या को 525 से 545 और एक राज्य के प्रतिनिधियों की ऊपरी सीमा को 500 से 525 तक बढ़ाया गया। |
| छत्तीसवें संशोधन | 1975 | सिक्किम को भारत संघ का राज्य बनाया गया। |
| अड़तालीसवें संशोधन | 1975 | राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने के लिए प्रदान किया गया और राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्देशकों द्वारा अध्यादेशों के प्रमुख और किसी भी न्यायालय में इसका विरोध नहीं किया जा सकता था। |
| उनतीसवें संशोधन | 1975 | प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं की जा सकती है। |
| बयालीसवें संशोधन | 1976 | संसद को प्राथमिकता और निर्देशन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रभुत्व दिया गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और संविधानप्रांबल में परिवर्तन किया गया। |
| चौंचालीसवें संशोधन | 1978 | लोकसभा और विधान सभाओं की सामान्य अवधि को 5 वर्षों तक पुनर्स्थापित किया, अधिकार के अधिकार को भाग III से हटाया और आंतरिक आपातकाल की प्रविष्टि को सीमित किया। |
| पैंतालीसवें संशोधन | 1980 | SC/ST के लिए आरक्षण को अतिरिक्त 10 वर्षों तक बढ़ाया गया (1990 तक)। |
| बावीसवें संशोधन | 1985 | दलबदलुता के कारण त्याग के आधार पर अधिकारों की अविभाज्यता के लिए संविधान में दसवीं कार्यसूची सम्मिलित की गई। |
| पचीसवां संशोधन | 1986 | अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और संघ टेरिटरी गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। |
| इक्याईसवां संशोधन | 1989 | लोकसभा और राज्य विधान सभा के लिए मतदान आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। |
| तिरानवें संशोधन | 1992 | पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम सभा, पंचायतों के सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, SC और ST के लिए सीटों की आरक्षण और पंचायतों की कार्यकाल की 5 वर्षों तक नियमित करने के लिए प्रावधानिक है। |
| चौहत्तरवां संशोधन | 1993 | महापौरिका के तीन प्रकार, SC/ST, महिला और OBC में सीटों की आरक्षण के लिए प्रावधानिक है। |
| सत्ताईसवां संशोधन | 1995 | SC/ST के पदोन्नति के लिए आरक्षण की नीति को जारी रखने और धारा 16 के नए धारा (4A) में परिवर्तन करने के लिए नया धारा (4A) संशोधित किया गया। |
| उनासीवां संशोधन | 1999 | लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में SC/ST और एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण को अतिरिक्त 10 वर्षों तक बढ़ाया गया। |
| छियासीवां संशोधन | 2002 | धारा 21A सम्मिलित करके, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। |
| उननवे संशोधन | 2003 | अनुसूचित जातियों की राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों की राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने के लिए धारा 338 में संशोधन किया गया। |
| नब्बे संशोधन | 2003 | निश्चित राज्यों की विधान सभाओं में सीटों की संख्या प्रदान करने के लिए धारा 170A सम्मिलित किया गया। |
| एकानवे संशोधन | 2003 | मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को सीमित करने के लिए धारा 75 में संशोधन किया गया। |
| बानवे संशोधन | 2003 | बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया। |
| तिरपन्वे संशोधन | 2006 | सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया गया। |
| उनानवे संशोधन | 2014 | राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की प्रावधानिक है (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द की गई)। |
| सौ संशोधन | 2015 | भारत और बांग्लादेश के बीच भू-सीमा समझौते (LBA) से संबंधित है। |
| सौ एक और एकवां संशोधन | 2016 | वस्त्र और सेवा कर (GST) को लागू करने के लिए लाया गया। |
| सौ तिरेंद्र व संशोधन | 2019 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों में और केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया। |
| एक सौ चौथवां संशोधन | 2020 | लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में SCs और STs के लिए सीटों की आरक्षण को विस्तारित किया गया। |
| एक सौ पाँचवां संशोधन | 2021 | इसने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की पहचान करने की राज्य सरकारों की शक्ति को पुनर्जीवित किया। |
| एक सौ छठवां संशोधन | 2023 | यह लोकसभा, राज्य विधान सभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। |
संविधान संशोधन का महत्व
भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधानों के महत्व को नीचे समझाया गया है:
- शासन व्यवस्था में अनुकूलता: संविधान शासन के मौलिक सिद्धांत निर्धारित करता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और लगातार विकसित हो रहे देश को कुछ निश्चित नियमों द्वारा शासित नहीं किया जा सकता। संविधान का संशोधन आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाने में सक्षम बनाता है।
- नये अधिकारों का समायोजन: बढ़ती जागरूकता के साथ, समाज के विभिन्न वर्ग अपने अधिकारों के प्रति मुखर हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में LGBT समुदाय अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। संशोधन ऐसे अधिकार प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- नये अधिकारों का विकास: संविधान की नई व्याख्याओं के कारण नए अधिकारों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की एक नई व्याख्या ने निजता के अधिकार को जन्म दिया। संशोधन ऐसे अधिकारों को समायोजित करने में सक्षम बनाता है।
- उभरते हुए मुद्दों का समाधान: यह नए उभरते रुझानों जैसे प्रतिबंध, सतर्कता आदि को संबोधित करने में सक्षम बनाता है।
- सामाजिक सुधार लाना: यह आधुनिकता लाने के लिए पुरानी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं के उन्मूलन को सक्षम बनाता है।
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बदलती सामाजिक जरूरतों और परिस्थितियों के लिए भारत के कानूनी ढांचे की प्रासंगिकता और अनुकूलन क्षमता को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन संवैधानिक संशोधनों ने देश के शासन और कानूनी ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।



 संसद के सदस्य, देखें संक्षिप्त परिचय...
संसद के सदस्य, देखें संक्षिप्त परिचय...
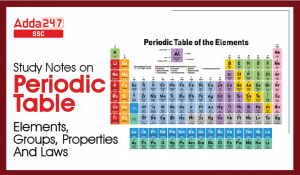 आवर्त सारणी: तत्व, समूह, विशेषता और इसके...
आवर्त सारणी: तत्व, समूह, विशेषता और इसके...
 भारत की महत्वपूर्ण झीलें : भारत की सबसे ...
भारत की महत्वपूर्ण झीलें : भारत की सबसे ...


